मैं हेलन पर फ़िल्म लिखना पसंद करूँगा- तेजेंद्र शर्मा

तेजेन्द्र शर्मा लम्बे अरसे से लंदन में रह रहे हैं। इनके परिचय की जरूरत नहीं किसी को। बस इतना समझ लीजिए कि देश-विदेश के कई विश्वविद्यालयों में इनकी लिखी कहानियाँ और उपन्यास बतौर पाठ्यक्रम जुड़े हुए हैं। करीब दर्जनभर से ज्यादा इनके लिखे पर शोध हो चुका है। लंदन प्रिंस और भारत देश कई प्रधानमंत्री इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। एक समय दूरदर्शन के लिए चर्चित ‘शांति’ धारावाहिक भी लिखा। आज गंगानगर वाला उनसे कुछ सवाल-जवाब कर आपके सामने कुछ बातें लेकर आया है। तो लीजिए पढ़िए आखिर क्यों कह रहे हैं- मैं हेलन पर फ़िल्म लिखना पसंद करूँगा- तेजेंद्र शर्मा।
सिनेमा में महिलाओं की भूमिका को कितना अहम मानते हैं?
तेजेंद्र शर्मा- हिन्दी सिनेमा एक नायक प्रधान गतिविधि रही है। कुंदन लाल सहगल से लेकर ऋतिक रौशन तक पहला ध्यान हमेशा फ़िल्म के नायक की ओर जाता है। फ़ाइनेंस उसके नाम से मिलती है और दर्शक भी। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि महिलाओं की भूमिका सिनेमा के लिये अहम नहीं है। यूँ साल 1936 की फ़िल्म अछूत कन्या से नारी केन्द्रित फ़िल्में बननी शुरू हो गईं थीं। नरगिस, नूतन, मीना कुमारी, मधुबाला, वहीदा रहमान, वैजयन्ती माला, साधना, शर्मिला टैगोर, राखी, शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल और दीप्ति नवल जैसी तमाम कलाकारों ने बहुत सी ऐसी फ़िल्मों में अभिनय किया जिनके केन्द्र में नारी पात्र होते थे। यह आवश्यक नहीं कि केन्द्र में महिला पात्र हो ऐसी भी बहुत सी फ़िल्में बना करती थीं जिनमें बड़े सितारों के साथ भी महिला कलाकार बराबर की टक्कर देती थीं। ‘आवारा’ और ‘श्री 420’ में नरगिस ने राजकपूर के मुकाबले अपने आपको कहीं उन्नीस नहीं होने दिया। ठीक वैसे ही वैजयन्ती माला और वहीदा रहमान ने दिलीप कुमार और देव आनंद के साथ। शबाना, स्मिता और दीप्ति नवल ने तो समानांतर सिनेमा के आंदोलन में एक से बढ़ कर एक किरदार निभाए। बाद की पीढ़ी में करिश्मा कपूर, जूही चावला, करीना कपूर, काजोल, प्रीति ज़िन्टा आदि ने अपनी हर फ़िल्म में नायक के मुक़ाबले अपने किरदारों का महत्व बनाए रखा है।
महिला केन्द्रित फ़िल्मों ने फेमिनिज़्म को किस हद तक बढावा दिया है?
तेजेंद्र शर्मा- सिनेमा और साहित्य में एक मूलभूत अंतर है कि साहित्य एक व्यक्ति अकेला बैठकर लिखता है जबकि सिनेमा का निर्माण और पहुँच बहुत दूर तक की है। इसलिये सिनेमा को किसी विमर्श में बांध पाना आसान नहीं। सिनेमा के साथ बहुत से कारीगरों की रोटी-रोज़ी जुड़ी रहती है। इसलिये सिनेमा किसी ‘इज़्म’ को ध्यान में रख कर नहीं बनाया जाता। जो सिनेमा इस उद्देश्य से बनाया जाता है उसकी पहुँच बहुत कम लोगों तक रहती है। हाँ सिनेमा महिलाओं को नये-नये फ़ैशन अवश्य सिखाता रहा है। कभी तंग पजामी है तो कभी बैल-बॉटम, कभी स्कर्ट है तो कभी साड़ी। शारदा, ख़ामोशी, रात और दिन, तपस्या, दाग़, अर्थ जैसी फ़िल्में गंभीर होती हैं। उनके किरदारों जैसा बन पाना कठिन होता है। हाँ यह सच है कि जिन फ़िल्मों में बोल्ड सीन होते हैं, महिलायें यदि उसी को फ़ेमिनिज़्म समझ बैठें तो उस हद तक सिनेमा प्रेरित करता है। मगर सिनेमा से किसी ‘इज़्म’ की अपेक्षा करना ग़लत होगा।
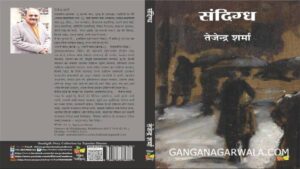
फ़िल्मों में नायिका प्रधान फ़िल्में जिन्हें कह सकते हैं, से प्रेरित होकर आने वाली नई अभिनेत्रियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
तेजेंद्र शर्मा- नायिका प्रधान फ़िल्में आम तौर पर नारी के संघर्ष और उपलब्धियों की गाथा कहती है। ऐसी फ़िल्मों में पेड़ों के इर्द-गिर्द नाचने-गाने का अवसर नहीं मिलता। ‘नूतन’ की सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरी आंगन की, ‘शर्मिला टैगोर’ की मौसम, ‘नरगिस’ की रात और दिन, ‘वहीदा रहमान’ की ख़ामोशी, तीसरी कसम और गाइड, ‘राखी’ की तपस्या कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जिन्हें हर उभरती हुई कलाकार को देखना ही चाहिये। उनकी अदाकारी इतनी पारदर्शी होती है कि नये कलाकारों को इनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल सकता है। सिनेमा में संवाद अदायगी ही अभिनय नहीं होता। रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया देना अभिनय का एक बहुत ही ख़ूबसूरत पहलू है। जब सुजाता में टेलिफ़ोन पर एक तरफ़ सुनीत दत्त तलत महमूद की आवाज़ में गीत गा रहे होते ‘हाँ- जलते हैं जिसके लिये, तेरी आँखों के दिये’, तो फ़ोन की दूसरी तरफ़ नूतन केवल रिएक्शन देकर पूरे गीत का स्तर उठा देती हैं। बिना संवाद बोले अदाकारी करने की कला पुरानी अभिनेत्रियों में जैसे कूट-कूट कर भरी थी। अनुपमा में शर्मिला टैगोर पूरी फ़िल्म में लगभग ख़ामोश रहकर केवल आँखों से अदाकारी करती हैं।
भारतीय फ़िल्म उद्योग में महिला निर्माता, निर्देशक की भूमिका को कितना अहम और जरूरी मानते हैं?
तेजेंद्र शर्मा- एक ज़माना था जब समाज का हर काम केवल पुरुष ही किया करते थे। महिलायें घर संभाला करती थीं और बाहर का काम देखते थे पुरुष। समय बदला, महिलाओं ने घर से बाहर कदम निकाला और आहिस्ता-आहिस्ता बाहर के कामों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी शुरू की। फातिमा बेगम भारतीय सिनेमा की पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थीं जिन्होंने 1926 में ‘बुलबुल-ए-परिस्तान’ फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। समय के साथ-साथ और नाम भी जुड़ते चले गये। कई अभिनेत्रियां ऐसी भी आईं जिन्होंने अभिनय के साथ-साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया। इनमें थीं- शोभना समर्थ, साधना, तब्बसुम, हेमामालिनी, नीलिमा अजीम, सोनी राजदान, नंदिता दास और पूजा भट्ट। इन सभी अभिनेत्रियों ने निर्देशन के लिए या तो अभिनय क्षेत्र को त्याग दिया या फिर दोनों ही काम को बराबर करती रहीं।

पिछले दो-तीन दशकों में कुछ मशहूर महिला निर्देशकों को याद करें तो उनमें विजया मेहता, साईं परांजपे, अपर्णा सेन, अरूणा राजे, दीपा मेहता, कल्पना लाजमी, मीरा नायर, गुरविदंर चड्ढा, फराह खान, तनुजा चंद्रा, विंता नंदा, लीना यादव, फ़रहा ख़ान, जोया अख्तर, किरण राव, सोहना उर्वशी, मेघना गुलजार, रीमा राकेशनाथ, बेला नेगी, जेनिफर लिंच, सौंदर्य रजनीकांत, लवलीन टंडन, रीमा कागती और गौरी शिंदे के नाम उभर कर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी को अलग से महिला के रूप में रेखांकित करने की आवश्यकता है।
भारतीय फ़िल्म उद्योग में संगीत निर्देशिकाएं, पटकथा लेखिकाएं आदि नहीं हैं। क्या महिलाएँ आज भी अदाकारी के नाम पर दिखावे का प्रतीक है?
तेजेंद्र शर्मा- सिनेमा का संगीत एक स्पेशलाइज़ड काम होता है। जहाँ कोई आरक्षण जैसी सुविधा नहीं होती है। सिनेमा के इस फ़ील्ड के लिये अलग किस्म की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। संगीत निर्देशन के मुकाबले एक्टिंग अधिक सुविधाजनक और लोकप्रियता दिलवाने वाला काम है। वैसे तो सरस्वती देवी और जद्दनवाई ने फ़िल्मों में संगीत दिया, एक और संगीतकार ‘बिब्बो’ भी हुआ करती थीं। मगर सही मायने में पुरुष संगीतकारों को टक्कर देने का काम उषा खन्ना ने ही किया। जब से सिनेमा में गीतों की शुरूआत हुई, शायद दस से अधिक महिला संगीतकारों का नाम नहीं सुनाई दिया। और मज़ेदार बात यह भी है कि उषा खन्ना हिन्दी सिनेमा में गायिका बनने के लिये आईं थीं मगर बन गईं संगीतकार। उनके संगीत में हर बड़े गायक ने आवाज़ दी। मुहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, मन्ना डे, मुकेश सभी ने कोई-न-कोई बेहतरीन गीत उषा खन्ना के संगीत में गाया। इसी तरह सिनेमा के हर फ़ील्ड में कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर, संवाद लेखक, गीत लेखक, पटकथा लेखिकाएं महिलाओं की कमी तो है ही। लेकिन जैसे महिलाओं ने अध्यापन के क्षेत्र को चुना, सिनेमा में अदाकारी उनकी पहली पसन्द थी। वैसे अरुणा ईरानी, अचला नागर, अनु मेनन, अनुराधा तिवारी, जूही चतुर्वेदी, इला बेदी (राजेन्द्र सिंह बेदी की पोती), अद्वैता काला और उर्मि जुवेकर जैसे कुछ नाम हैं जो सिनेमा के लिये पटकथा लिख रहे हैं। फ़िल्में बहुत तरह की बनती हैं। किसी में महिला किरदार केवल शोपीस होते हैं और कुछ अन्य फ़िल्में होती हैं जिनमें उनके किरदार अपनी उपस्थिति मौजूद करवाते हैं। एक ज़माना था रेहाना सुल्तान के नाम पर ही फ़िल्म चलती थी- चेतना और दस्तक तो अपने ज़माने की नई लहर जैसी फ़िल्में थीं।
हिंदी फ़िल्मों में मुख्य रूप से दो धाराएँ हैं एक धारा उन फ़िल्मों की जिनमें महिलाएँ पुरुष नायकों की प्रेमिकाएँ बनकर रह गईं तो दूसरी ओर बेग़मजान, राज़ी जैसी नायिकाएँ लिहाजा सिनेमा में इस बंधे बंधाएं पैटर्न के इतर भी कोई तीसरी धारा हो सकती है?
तेजेंद्र शर्मा- हमारे यहाँ एक पूरा ट्रैडीशन है ऐसी फ़िल्मों का जिनमें महिला कलाकारों के लिये मज़बूत रोल लिखे जाते थे। ‘मदर इंडिया’ की परंपरा खत्म नहीं हुई। बिमल रॉय, गुरुदत्त, राज कपूर, एल. वी. प्रसाद, जेमिनी, चेतन आनंद, श्याम बेनेगल और वर्तमान में किरण रॉव ऐसी फ़िल्में बनाते हैं जिनमें हिरोइन केवल हीरो की प्रेमिका नहीं होती। यहां तक की गंगा-जमुना जो दो भाइयों की कहानी थी, उसमें भी वैजयन्ती माला का चरित्र केवल हीरो की प्रेमिका का नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फ़िल्मों में कभी भी महिला चरित्रों को भर्ती का चरित्र नहीं बनने दिया। यहां तक कि कमर्शियल फ़िल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी का किरदार धर्मेन्द्र और संजीव कुमार से कहीं अधिक सशक्त था। एक तीसरी धारा हमेशा से मौजूद थी, जो शायद सरस्वती की तरह हमारी नज़रों से ओझल रही। मगर गंभीरता से देखने पर हमेशा दिखाई देती है।
तेजेंद्र शर्मा का चर्चित कहानी संग्रह मौत… एक मध्यांतर अमेजन की इस लिंक से ख़रीदा जा सकता है।

फ़िल्मों में गीतों को लें तो आज के समय में गीत मर रहे हैं ऐसा लता मंगेशकर ने भी एक बार कहा था। क्या आप मानते हैं कि अब पहले जैसे सदाबहार गीत अब हमारे गीतकारों के पास नहीं है?
तेजेंद्र शर्मा- तेजस, हर पीढ़ी की अपनी-अपनी पसंद होती है। हमारे बुज़ुर्ग के. एल. सहगल, जगमोहन, पंकज मलिक, के.सी. डे, पहाड़ी सान्याल के गीत गुनगुनाया करते थे। उन्हें 1950 के बाद के गीत हल्के लगते थे। मेरा निजी मानना है कि 1950 से 1970 के बीच हिन्दी सिनेमा का स्वर्णकाल था। इस दौरान बेहतरीन गीत लिखे गये और संगीत भी अद्भुत था। जैसे-जैसे जीवन की गति बढ़ी उसी के साथ-साथ संगीत और गीत भी बदले। अंग्रेज़ी में कहावत है कि “पास्ट इज़ ऑलवेज़ ग्लोरियस!” वो यहां भी लागू होता है। चलिये साहित्य की बात करते हैं। क्या आपको आज निराला, पंत, प्रसाद जैसे कवि सुनाई देते हैं। उन्हें तो छोड़िये क्या नीरज जैसे कवि मौजूद हैं आजकल? कविता में से तुक ख़त्म हो गई है। यदि मुख्यधारा के साहित्य का यह हाल है तो भला सिनेमा इससे अछूता कैसे रह सकता है। अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने में किसी भी फ़िल्म की सफलता का पैमाना होता था उसका सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली होना। यानी कि फ़िल्म छः महीने से एक साल तक सिनेमा हल में चलती रहती थी। मगर अब फ़िल्में एक सप्ताह में अपनी लागत वसूल करके मुनाफ़ा भी कमा लेती हैं। जब फ़िल्म ही चार सप्ताह में उतरने वाली है तो उसके गीत भी तो उसी तरह ज़बान से उतर जाएंगे। वैसे इस बारे में राजकपूर ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, “पहले जब गीत बजते थे, तो सिर हिलता था… आजकल पाँव हिलते हैं।”
हिंदी फ़िल्मों में महिलाएँ जो स्टंट करती हैं उन्हें पुरुषों के स्टंट के सामने कमतर क्यों आंका जाता है?
तेजेंद्र शर्मा- महिला कलाकारों के स्टंट तुलनात्मक रूप से सॉफ़्ट होते हैं। पुरुषों के स्टंट मार-धाड़ के अलावा ख़तरे से भरपूर होते हैं। पहले तो यह सोचा ही नहीं जा सकता था कि महिलाओं के लिये स्टंट की आवश्यकता हो सकती है। महिलाएं आमतौर पर पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाई जाती थी। फ़ीयरलेस ‘नाडिया’ तो अपने स्टंट स्वयं किया करती थीं। जब तक सीता और गीता, शोले जैसी फ़िल्में नहीं बनाई गईं, महिला स्टंट कलाकारों की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। और जब पुरुष स्टार को महिला स्टार से अधिक पैसे मिलते हैं, तब हम वैसा सवाल नहीं पूछते, तो फिर यहां क्यों।
यह भी पढ़ें- राजू हिरानी सफल फिल्मकार हैं- अजय ब्रह्मात्मज
वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण ने हिंदी फ़िल्म उद्योग में महिला अदाकाराओं को किस हद तक प्रभावित किया है?
तेजेंद्र शर्मा- वैश्वीकरण के बाद से विश्व सिनेमा भारत में आसानी से दिखाई दे जाता है। नेटफ़्लिक्स, अमेज़ॉन, सोनी और ज़ी-5 जैसे बहुत से प्लैटफ़ॉर्म हैं जहाँ भारतीय कलाकार बाहर की फ़िल्में देख पाते हैं और विदेशी फ़िल्म निर्माता भारतीय फ़िल्में देख पाते हैं। प्रियंका चोपड़ा को जिस तरह हॉलीवुड में एक्सपोज़र मिला है उससे नये रास्ते अवश्य खुलते हैं। अच्छी अदाकारी से परिचित होकर भारतीय सिनेमा में भी अभिनेत्रियां बेहतर से बेहतर अदाकारी का प्रदर्शन कर सकती हैं। प्रियंका क्योंकि मिस वर्ल्ड 2000 भी थीं, तो उन्हें मुंबई सिनेमा से हॉलीवुड पहुंचने में थोड़ी आसानी अवश्य हुई होगी।
भारतीय फ़िल्म उद्योग में सन्नी लियोन जो पोर्न स्टार के रूप में खूब प्रसिद्धि पा चुकी है क्या ऐसी लड़कियों की सच में हिंदी सिनेमा जगत को आवश्यकता है?
तेजेंद्र शर्मा- हिन्दी सिनेमा में आने से पहले बहुत से कलाकार कुछ-न-कुछ कर रहे होते हैं। कोई बस कंडक्टर होता है तो कोई वाचमैन। हम कभी यह सवाल नहीं पूछते कि उनके व्यवसाय से किसी को एक्टर बनना चाहिये या नहीं। फिर एक पोर्न स्टार से यह सवाल क्यों? सन्नी लियोन हिन्दी सिनेमा में पोर्न वाला काम तो नहीं कर रही। दिक्कत हम लोगों में है। हमारे दिमाग़ में सन्नी लियोन की एक इमेज बनी हुई है, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। यदि वह कलाकार अच्छी है तो चलेगी… यदि भावहीन है तो दो-चार फ़िल्मों के बाद घर बैठ जाएगी। किसी के पिछले कार्यक्षेत्र को लेकर उसके प्रति पूर्वाग्रह रखना सही नहीं होगा।
भारतीय फ़िल्म उद्योग में कास्टिंग काउच की क्या सच में आवश्यकता है और इसकी शिकार महिलाएँ जो आज आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं आने वाली अभिनेत्रियों के लिए कुछ सकारात्मक क्यों नहीं करती?
तेजेंद्र शर्मा- यह सवाल कुछ ऐसा आभास देता है जैसे हर कलाकार को सिनेमा में काम पाने के लिये कास्टिंग काउच के माध्यम से जाना एक लीगल प्रक्रिया है। क्या कभी कोई कह सकता है कि कास्टिंग काउच की आवश्यकता है? कास्टिंग काउच सिनेमा की एक कड़वी सच्चाई है मगर आवश्यकता नहीं। यदि दस महिला कलाकार कास्टिंग काउच के माध्यम से काम पा सकी हैं तो सैंकड़ों ऐसी भी हैं जो काउच तक गईं तो सही मगर कैमरे का मुँह नहीं देख पाईं। जब ‘मी टू’ का शोर मचा था तो बहुत सी फ़िल्मी हस्तियां बेनकाब हुईं थीं। मगर कास्टिंग काउच जैसा बदनुमा दाग़ सिनेमा के माथे पर लगा रहा… न जाने कब हटेगा। मामला डिमाण्ड और सप्लाई का है। काम मांगने वाले लोग अधिक हैं और काम कम है… इसीलिये ये शॉर्टकट इस्तेमाल किये जाते हैं। क्योंकि अभिनेत्रियां स्वयं फ़िल्में नहीं बनातीं, इसलिये उनके अधिकार क्षेत्र में कुछ सकारात्मक करना आता ही नहीं।
संजय दत्त पर बायोपिक बनी जिस तरह क्या बॉलीवुड में किसी महिला पर बायोपिक बनेगी अगर आप बायोपिक बनाते तो किस पर बनाते?
तेजेंद्र शर्मा- वैसे तो जयललिता के जीवन पर बायोपिक बन चुकी है- थलाइवी। इस फ़िल्म में जयललिता का किरदार कंगना रनौत ने निभाया था। फ़िल्म कलाकारों में से भी केवल संजय दत्त के जीवन पर ही बायोपिक बनी है। महिलाओं में मेरीकॉम, नीरजा भनोट, फूलन देवी आदि पर ही फ़िल्में बनाई गई हैं। फ़िल्म बनाने के लिये जीवन में ड्रामा होना अति आवश्यक है। केवल किसी सफल कलाकार पर फ़िल्म बनाना आसान नहीं होता है। यदि मुझे एक लेखक के रूप में पूछा जाए, तो मैं हेलन, मधुबाला और रेखा में से किसी एक पर फ़िल्म लिखना चाहूंगा। हेलन मेरी पहली पसन्द होगी।
तेजेंद्र शर्मा की किताब संदिग्ध अमेजन के इस लिंक से खरीदी जा सकती है।






सबसे पहले तेजस जी को सार्थक और समीचीन प्रश्न सृजितकरने के लिए। बहुदा हम एंकर यश सूत्रधार को भूल जाते हैं जबकि वहीं किसी भी साक्षात्कार का गणेश यानी विग्नेश्वर होता है अतः तेजस जी को बहुत-बहुत साधुवाद।
आदरणीय सुप्रसिद्ध प्रवासी साहित्यकार तेजिंदर शर्मा जी अब अमृत वर्ष के आसपास होंगे और वे हिंदी की अलख जगाने में पुरोधा समान हो गए हैं। नवोदित महिला कलाकारों पर कोई प्रश्न का न पूछा जाना थोड़ा सा अटपटा लगा।
प्रवासी भारतीय साहित्यकारों में उन्हें निसंदेह रूप से प्रवासी साहित्य और सिनेमा का प्रेमचंद कहा जा सकता है। सिनेमा के सारे रंग इस संवाद में बिखरे और निखरे हैं। साहित्य और सिनेमा की यात्रा का मज़ा भी है और महिलाओं की समय दर समय स्थितियों का ईमानदार आकलन भी है। हेलेन हेलेन जैसी सुप्रसिद्ध महिला कलाकार का जिक्र और वह भी फिक्र के साथ हो इसे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि इस कलाकार में भारतीय समाज की कलात्मक कामुकता मादकता यवन की संकल्प मस्ती क्या-क्या नहीं शोकेस किया है सहकार के रूप में सरकार किया है भगमों के रूप में अभिनय के रूप में सब हो देखा जाए तो हेलेन पर यदि कोई पिक्चर बनती है तो वह बर्मा से लेकर और हिंदुस्तान और बॉलीवुड की खुशबू को साथ लिए होगी।
अस्तु कुल मिलाकर एक बहुत बेहतरीन या उर्दू भाषा में कहें तो आफ़रीन इंटरव्यू रहा है ।धन्यवाद दोनों को
बहुत आभार आपका। सूर्यकांत जी। आपने एक जिज्ञासा नवोदित कलाकारों को लेकर की है इस पर भी सवाल बनाए जाएंगे भविष्य में। आभार पुन: पढ़ते पढ़ाते रहें
फिल्मों का गहरा शोध और ज्ञान है तेजेन्द्र जी को। बहुत सधे और सटीक उत्तर हैं। हेलेन की बता करके एक bold तड़का भी लगाया है।बधाई और शुभकामना तेजस जी और तेजेन्द्र जी।
शुक्रिया पढ़ते पढ़ाते रहें।
काफी बड़ा, लंबा, गहरा और सधा हुआ इंटरव्यू रहा यह। यहां हम दोनों की ही तारीफ करना चाहेंगे।तेजस जी के लिए तो उनकी तैयारी के लिए शाबाशी है। जो-जो और जितने प्रश्न उन्होंने उठाए, उसकी तैयारी के लिए तो आप वाकई शाबाशी के पात्र हैं।
और तेजेन्द्र जी के लिए- सबसे पहले तो हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। उन्होंने बहुत ही सधे, संतुलित और सटीक लंबे -लंबे प्रश्नों के लंबे-लंबे जवाब शालीनता के साथ, पता नहीं कितना सारा धैर्य रखकर दिये।
पढ़ते हुए कुछ उत्सुकता मन में जागी।
-इंटरव्यू की अवधि कितनी थी? क्योंकि जितना हमने तेजेन्द्र जी को सुना है, उन्हीं को अपनी कहानी सुनाते हुए और जो कुछ इंटरव्यू उनके हमने देखे, बहुत ही धीरे-धीरे बहुत ही सोच समझकर वह अपनी बात को रखते हैं। तो क्या आपका इंटरव्यू अपनी अवधि में समाप्त हो पाया?
हम तो बहुत अधिक फिल्में नहीं देख पाते थे लेकिन फिर भी हमें याद है की जैमिनी नाम से हम दूसरी क्लास से ही पढ़ते थे और उसके बाद भी शांताराम इन दो की फिल्में अक्सर हम लोग देखते थे अगर छुट्टियों में लगी मिल जाती थी तो। तो फिल्मों की जानकारी तो खैर हमें ज्यादा नहीं है लेकिन तेजेन्द्र जी को पढ़कर काफी कुछ जाना फिल्मों को लेकर यह शायद उनका दूसरा या तीसरा इंटरव्यू है जो हमने देखा। और फिल्मी जानकारी का इतना अंबार आश्चर्यचकित करता है।
इसमें कोई दो मत नहीं की 50 से 70 तक के दशक में जो गाने थे वह आज भी जबान पर हैं।
और इस बात से भी सहमत हैं कि पहले के गानों पर सिर हिला करते थे और आजकल के गानों पर पर पैर हिला करते हैं।
शुक्रिया तेजस जी आपका आपकी बदौलत फिल्मी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जाना।
आभार पढ़ते पढ़ाते रहें। इतनी विस्तृत टिप्पणी के लिए शुक्रिया। और यह मौखिक रूप से वार्तालाप नहीं हुई थी मैंने उन्हें सवाल भेजे थे और उन्होंने जवाब। जिन्हें बाद में प्रूफ करके प्रकाशित किया गया है।